रक्त की एक-एक बूंद बेशकीमती होती है क्योंकि ब्लड किसी लैब या फैक्ट्री में नहीं बन सकता। जब कोई डोनर अपना ब्लड देता है तब जाकर किसी एक इंसान की जान बचती है। अपने देश में हर दो सेकेंड में किसी को खून की जरूरत पड़ती है, लेकिन कई बार खून न मिलने से लोगों की जान चली जाती है।
क्या आपको पता है कि 375 एम एल का एक ब्लड बैग तीन लोगों की जान बचा सकता है। पर हकीकत यह है कि देश में हर साल छह लाख लीटर से अधिक खून बर्बाद हो जाता है। बता दें कि भारत में एक हजार लोगों में से केवल 8 लोग ही स्वैच्छिक रूप से ब्लड डोनेट करते हैं।
आज ‘वर्ल्ड ब्लड डोनर डे’ है। देश में वैसे ही ब्लड डोनेट करने वालों की गिनती कम है, लेकिन डोनेट किया गया ब्लड किस तरह बर्बाद हो जाता है और उसके पीछे क्या कारण हैं, यह जानना जरूरी है।
ब्लड बैंकों में स्टोरज की क्षमता कम, खून बर्बाद हो जाता है
देश भर में 3840 लाइसेंसी ब्लड बैंक हैं जिनमें से महज 1244 ब्लड बैंक ही सरकारी हैं। यानी 68% से ज्यादा ब्लड बैंक प्राइवेट हैं या फिर एनजीओ चला रहे हैं।
ब्लड डोनेशन के लिए कैंपेन चलाने वाले ‘लाइफ सेवर्स’ के फाउंडर अतुल गेरा ने बताया कि सरकारी या प्राइवेट, अधिकतर ब्लड बैंकों में ब्लड स्टोरेज की क्षमता कम है। मैनपावर कम होने से खून की जांच में काफी समय लगता है। नतीजा, डोनेट किए गए खून का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है।
इसलिए जब मेगा ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं तो स्टोरेज की क्षमता से ज्यादा खून जमा हो जाता है जिसे स्टोर करना मुश्किल होता है।
उन्होंने बताया कि पिछले साल 87 हजार से अधिक लोगों ने एक दिन में स्वैच्छिक रक्तदान किया था, लेकिन इसे स्टोर करने के लिए महज 3840 ब्लड बैंक काफी नहीं हैं।
ब्लड बैंकों में ब्लड कंपोनेंट्स यानी रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स को अलग करने के लिए मशीनें भी पर्याप्त नहीं हैं। न ही ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए टेंपरेचर का एडवांस सेटअप ही है।
देश में 1.25 करोड़ यूनिट ब्लड स्टोरेज है, लेकिन डिमांड 1.46 करोड़ यूनिट की है। इसमें से भी करीब 6% ब्लड बेकार हो जाता है।
डोनेट किया हुआ कितना ब्लड बर्बाद हो जाता है इसे ‘इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंटेम्पररी मेडिकल रिसर्च’ में छपी एक रिसर्च से समझ सकते हैं। रिसर्च एक रूरल ब्लड बैंक सेंटर में की गई।
डोनेट किए ब्लड की होती है पांच तरह से जांच
डोनेट किए गए ब्लड की पांच तरीके की जांच अनिवार्य रूप से होती है। पीजीआई चंडीगढ़ के ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट के हेड डॉ. आरआर शर्मा ने बताया कि जब किसी ब्लड बैंक को ब्लड डोनेट होता है तो HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, मलेरिया और सिफलिस की जांच की जाती है।
केंद्र सरकार की ओर से इस पर एक गाइडलाइन भी बनाई गई है। ये पांचों जांच किए बिना किसी भी ब्लड को स्टोर नहीं किया जा सकता।
- जांच में किसी भी इन्फेक्शन के पॉजिटिव आने पर खून को डिस्कार्ड करना पड़ता है
किसी भी डोनर का ब्लड लेते समय उसकी मेडिकल हिस्ट्री पूछी जाती है। कई बार लोग कई बातें छिपा लेते हैं। कई को यह पता ही नहीं होता कि उसे HIV है या हेपेटाइटिस बी या सी है। डॉ. आरआर शर्मा ने बताया कि इन पांचों जांच में किसी में भी रिजल्ट पॉजिटिव आया तो ब्लड को डिस्कार्ड करना पड़ता है।
- दूषित ब्लड का क्या करते हैं?
ब्लड बैंकों में टेस्ट के दौरान यदि खून दूषित पाया जाता है तो इसे बैक्टीरिया या वायरस मुक्त किया जाता है। जिस मशीन में दूषित खून को डाला जाता है उसे ऑटोक्लेव मशीन कहते हैं। इसका आकार सिलेंडर जैसा होता है जो किसी प्रेशर कुकर की तरह काम करता है।
दूषित खून को इसमें डाला जाता है जिसका तापमान 120 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें आधे से पौन घंटे तक खून को रखने पर यह एक तरह से पाउडर में तब्दील हो जाता है। यह किसी काम का नहीं रहता।
इससे संक्रमण होने का भी रिस्क नहीं रहता। बावजूद इसके, इसे एहतियातन उन अस्पतालों या आउटसोर्सिंग एजेंसी को भेज दिया जाता है जहां इंसीनिरेटर होता है। वहां इसे पूरी तरह जला दिया जाता है।
सवाल यह उठता है कि क्या जांच के दौरान दूषित पाए जाने पर ही ब्लड वेस्टेज होता है या इसके और भी कारण हैं। यह जानने से पहले यह ग्राफिक देख लेते हैं-
- बच्चों के लिए भी खून की बड़ी थैली इस्तेमाल होती है, इससे भी वेस्टेज
देश में ब्लड वेस्टेज का एक बड़ा कारण पीडियाट्रिक्स ब्लड बैग्स या पेंटा बैग्स (बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाली खून की छोटी थैली) की कमी है।
दिल्ली स्थित सीताराम भरतिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च के पीडियाट्रिक कंसल्टेंट डॉ. एचपीएस सचदेवा ने बताया कि कोई भी बच्चा जिसका वजन 10 किलो से कम है उसे 100 एमएल से ज्यादा ब्लड की जरूरत नहीं होती। इसी तरह नवजात के लिए 30 एमएल ब्लड पर्याप्त है, लेकिन इनके लिए भी 350 एमएल यानी बड़े लोगों के लिए जो खून की थैली होती है वही मंगाई जाती है।
‘लाइफ सेवर्स’ के फाउंडर अतुल गेरा ने बताया कि रांची, पटना, लखनऊ, गुवाहाटी, भोपाल, इंदौर, जयपुर जैसे बड़ों शहरों में भी अधिकतर प्राइवेट ब्लड बैंकों में पेंटा बैग्स नहीं होते।
हालांकि कुछ ही सरकारी ब्लड बैंकों में ये छोटी थैलियां होती हैं। नतीजा खून बर्बाद होता है।
डॉ. आरआर शर्मा बताते हैं कि ब्लड बैंक चलाने वाली एजेंसी, एनजीओ या दूसरे अस्पतालों में जागरूकता की कमी है। खून की छोटी थैलियां बनाना कोई बड़ी बात नहीं है।
ब्लड बैंकों और अस्पतालों में डिमांड के हिसाब ये पेंटा बैग्स बनाए जा सकते हैं।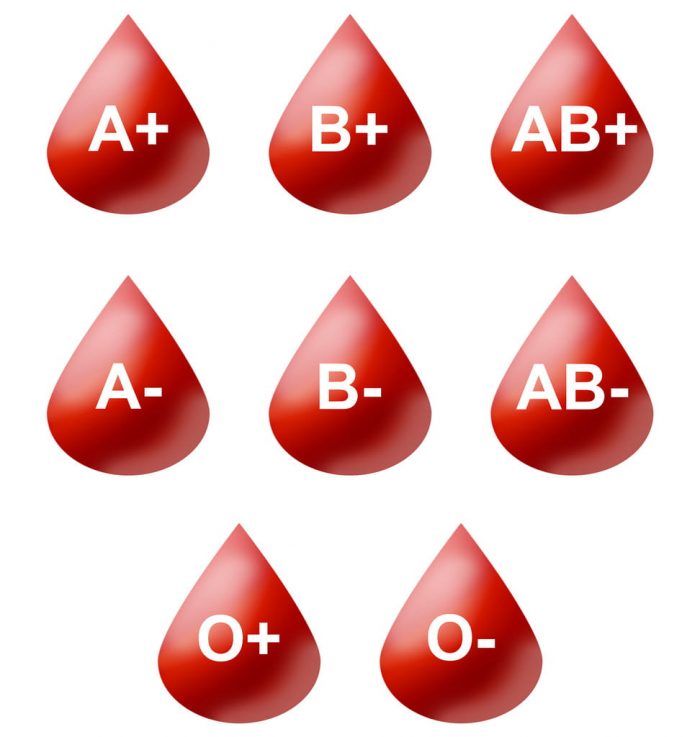
- थैलेसीमिया मरीजों को एक साल में चाहिए 20 लाख यूनिट ब्लड
भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हैं। करीब डेढ़ लाख बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित हैं और हर साल 10 से 15 हजार बच्चे इस बीमारी के साथ जन्म लेते हैं।
थैलेसीमिया एक जेनेटिक रोग है जो माता या पिता या दोनों के जीन्स में गड़बड़ी के कारण होता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन दो तरह के प्रोटीन से बनता है- अल्फा और बीटा ग्लोबिन।
इन दोनों में से किसी प्रोटीन के निर्माण वाले जीन्स में गड़बड़ी होने पर थैलेसीमिया की बीमारी होती है। इसमें शरीर में खून की कमी हो जाती है। रेड ब्लड सेल्स महज 20 दिनों में ही मरने लगते हैं। ऐसे मरीजों को तत्काल खून चढ़ाना पड़ता है।
डॉ. सचदेवा बताते हैं कि थैलेसीमिया के मरीजों को हर साल करीब 20 लाख यूनिट ब्लड की जरूरत होती है। चूंकि इनमें सबसे अधिक बच्चे होते हैं इसलिए यहां भी 350 एमएल वाली खून की थैली दी जाती है। जबकि बच्चों को खून की इतनी मात्रा की जरूरत नहीं होती। इसलिए यहां भी ब्लड की वेस्टेज होती है।
- बिना जरूरत के ही डॉक्टर ब्लड मंगा लेते हैं
अस्पताल में सर्जरी या किसी और ट्रीटमेंट के लिए कितना खून चाहिए, यह स्पष्ट नहीं होता। कई बार डॉक्टर बिना जरूरत के ही अधिक मात्रा में ब्लड मंगा लेते हैं।
बिहार के गोपालगंज के रहने वाले रोहित राय ने फोन पर बताया कि उनकी मौसी का कैंसर का इलाज पटना में चल रहा था। डॉक्टर ने तीन यूनिट ब्लड चढ़ाने की बात कही। किसी तरह तीन यूनिट ब्लड दिया गया, लेकिन इनमें से केवल एक यूनिट ब्लड ही चढ़ाया गया।
अतुल गेरा बताते हैं कि देश के लगभग सभी शहरों में यही हाल है। कैंसर, गायनेकोलॉजी, सर्जरी जैसे विभाग में डॉक्टर एहतियातन ब्लड मंगा लेते हैं जिसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि बचा हुआ ब्लड वापस ब्लड बैंक नहीं जाता।
ब्लड बैंक अपनी चौखट से बाहर होते ही ब्लड को वापस लेने से इनकार देते हैं।
ऐसे में बचे हुए ब्लड को वॉश बेसिन में यूं ही बहा दिया जाता है। इसे फेंकते समय भी सही से ध्यान नहीं रखा जाता। इस ब्लड के संपर्क में आने पर भी संक्रमण फैलने का खतरा रहता है।
अब एक नजर नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के एसओपी पर डाल लेते हैं जिसमें बताया गया है कि ब्लड बैंक से अस्पताल तक खून कैसे भेजा जाना चाहिए।
- प्लास्टिक की थैलियों में लाई जातीं खून की थैलियां
ब्लड बैंकों और अस्पतालों के बीच सही कोऑर्डिनेशन नहीं होता। जब मरीज को खून की जरूरत होती है तो उसके परिजन ब्लड बैंक से खून लाते हैं, लेकिन खून को अस्पताल तक लाने के लिए किसी तरह की कोल्ड चेन की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता।
प्लास्टिक की पन्नियों में खून की थैलियां ले जाई जाती हैं जिससे ब्लड की क्वालिटी खराब होने का डर रहता है।
डॉ. आरआर शर्मा ने बताया कि अगर ब्लड बैंक से खून लेकर अस्पताल जाते हैं तो इसे सेलो बॉक्स या थर्मोकोल के बॉक्स में रखा जाना चाहिए। साथ ही इसमें आइस पैक भी पर्याप्त हो ताकि टेंपरेचर कम रहे और हीमोग्लोबिन टूटे नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो खून ले जाने से बचना चाहिए।
इसी तरह यदि सर्जरी कल है और आज ब्लड मंगाया गया है तो इसे फ्रिज में कम से कम 4 डिग्री टेंपरेचर पर रखना होगा। अगर कोल्ड चेन को मेंटेन किया गया है तो ब्लड बचने पर इसे ब्लड बैंक को वापस किया जा सकता है।
इसके लिए डॉक्टर, नर्स और ब्लड बैंक के बीच समन्वय बैठाना जरूरी है।
- प्राइवेट अस्पताल कमीशन के लिए लिख देते हैं खून
अतुल गेरा बताते हैं कि ब्लड सप्लाई की आड़ में कई अस्पताल मोटी कमाई करते हैं। कई बार प्राइवेट अस्पताल 40% कमीशन के लिए ब्लड लिखते हैं जबकि इसकी जरूरत नहीं होती।
डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर प्राइवेट ब्लड बैंक का नाम लिखा रहता है।
मरीज के परिजनों पर दबाव होता है कि वे निजी ब्लड बैंक से ही खून लें। इसके लिए परिजनों को मोटी रकम देनी पड़ती है। जबकि ब्लड का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता।
अस्पतालों में खून दिलाने के लिए दलालों का बड़ा नेटवर्क काम करता है।
ब्लड और उसके कंपोनेंट को किस रेट पर अस्पतालों में सप्लाई किया जाता है इसे ग्राफिक से समझते हैं
- अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में 20% प्लेटलेट्स बर्बाद हो जाते हैं
अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों में भी ब्लड वेस्टेज रेट काफी अधिक है। कुल  जमा किए गए प्लेटलेट्स का 20% बेकार हो जाता है। दक्षिण अमेरिका देश गुयाना में यह 30% के करीब है।
जमा किए गए प्लेटलेट्स का 20% बेकार हो जाता है। दक्षिण अमेरिका देश गुयाना में यह 30% के करीब है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट के अनुसार, हाई इनकम कैटेगरी वाले देशों में ब्लड के बर्बाद होने की दर 5.7% है जबकि लोअर मिडिल इनकम वाले देशों में यह सबसे अधिक 10.9% है।
पूरी दुनिया में हर साल 1.50 करोड़ ब्लड बैग्स बेकार हो जाते हैं। इसका बड़ा कारण स्टोरेज फैसिलिटी में कमी और ट्रांसपोर्टेशन में जरूरी सुविधाएं न होना है।
रक्तदान को महादान कहा गया है। ऐसी बेशकीमती चीज जिससे किसी की जान बचती हो, उसका नष्ट होना हेल्थ सिस्टम पर सवाल खड़े करता है।
देश के ब्लड बैंक पहले से ही खून की कमी से जूझ रहे हैं। अगर इस ओर जागरूकता फैलाई जाए तो लाखों लोगों को समय पर ब्लड पहुंचाया जा सकेगा।
दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक
